प्राचीन भारत में आवर्त गतियों की समझ और इस ज्ञान का उपयोग
प्राचीन भारत में आवर्त गतियों की समझ और इस ज्ञान का उपयोग
यह शोधपत्र आकाश में देखी जा सकने वाली सूक्ष्म आवधिक गतियों के बारे में प्राचीन भारतीयों के ज्ञान से संबंधित है। यह शोध भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर भी देता है - विक्रम संवत (युग) का आरंभिक वर्ष 57 ईसा पूर्व क्यों है? इसका उत्तर पृथ्वी की धुरी के अग्रगमन के कारण वसंत विषुव के स्थानांतरण के ज्ञान, राशि चक्र के विभिन्न चिह्नों और भारत के ऐतिहासिक अभिलेखों से मिलता है।
परिचय
भारत में, दो सामान्यतः प्रयुक्त कैलेंडर हैं - पहला शक है जो 78 ई. से शुरू होता है जब दक्षिण भारत के शालिवाहन राजा ने मालवा के शक राजा को हराया था और दूसरा विक्रम कैलेंडर कहलाता है जो 57 ई.पू. से शुरू होता है। हालांकि, यह ज्ञात नहीं है कि इसे 57 ई.पू. से क्यों शुरू किया गया क्योंकि राजा विक्रमादित्य को व्यापक रूप से गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में स्वीकार किया गया है
इस कार्य का उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है।
भारत में कैलेंडर वर्ष और उनका आधार
भारतीय चंद्र कैलेंडर का पालन करते थे, जहां वर्ष को 27 या 28 भागों में विभाजित किया जाता था, और इनमें से प्रत्येक को नक्षत्र कहा जाता था [देवी, 1995]। नक्षत्र के दायरे में और भी उप-विभाजन थे। विभिन्न राशियों के आधार पर वर्ष को 12 महीनों में विभाजित करना बाद में प्रचलन में आया। इन राशियों और नक्षत्रों के आधार पर बारह महीनों के नाम एक विशेष राशि में सूर्य की स्थिति के कारण आए थे [शास्त्री और विल्किंसन, 1974]। यदि चंद्र मास की समाप्ति के बाद सूर्य उसी राशि में था, तो उस विशेष चंद्र मास में उसी नाम से अधिकमास नामक एक अतिरिक्त महीना होता था। महीनों के नाम पूर्णिमा के दिन विशेष नक्षत्र के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र हो तो उसे चैत्र माह कहा जाता था। इस प्रकार, सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच सामंजस्य स्थापित हो गया।
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति की चार महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञात थीं। ये घटनाएं थीं: वसंत और शरद विषुव, तथा शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन संक्रांति। चित्र 1 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा को दर्शाता है, जहां यह 21 जून को पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की स्थिति और दिशा को दर्शाता है [पेन-गैपोस्किन, और हरामुंडानिस, 1970]। इस समय, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। इसी तरह, 21 दिसंबर को, यह दक्षिणी ध्रुव होता है जो सूर्य की ओर झुका होता है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष सूर्य के केंद्र (हेलियोसेंट्रिक) पर परिभाषित एक त्रि-आयामी समन्वय प्रणाली के संबंध में समान अभिविन्यास बनाए रखती है। इस समन्वय प्रणाली के एक्स और वाई अक्ष क्रांतिवृत्त के तल में स्थित हैं। पृथ्वी का केंद्र सूर्य के चारों ओर घूमते समय इसी तल में घूमता है।
विषुव की स्थिति कक्षा पर उन बिंदुओं पर निर्धारित होती है जब पृथ्वी के दोनों ध्रुव सूर्य की किरणों से प्रकाशित होते हैं। ऐसा तब होता है जब यह अक्ष समन्वय प्रणाली के मूल से पृथ्वी के केंद्र तक खींची गई रेखा के लंबवत हो जाता है।
यद्यपि पृथ्वी की धुरी का अभिविन्यास किसी भी वर्ष में लगभग एक जैसा ही रहता है, फिर भी इसका अभिविन्यास लंबी अवधि में बदलता है, अर्थात अभिविन्यास परिवर्तन चक्रीय प्रकृति का होता है। इस परिवर्तन के एक चक्र में लगभग 25,800 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार, अत्यंत कम आवृत्ति की आवधिक गति के कारण आकाश में इस सूक्ष्म परिवर्तन को नोटिस करना वैदिक काल से ही भारतीय खगोलविदों द्वारा अर्जित एक बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान था [बर्गेस, 1977]। जहाँ तक यूनानियों के ज्ञान का सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के इस अग्रगमन का सबसे पहला वर्णन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में मिस्र में रहने वाले यूनानी हिप्पार्कस द्वारा किया गया है [एबेल, 1975]। इस घटना को चित्र 2 में दिखाया गया है, और इसे पृथ्वी के अक्ष का अग्रगमन कहा जाता है। पृथ्वी के भूमध्यरेखीय उभार पर चंद्रमा, सूर्य, आदि द्वारा ज्वारीय (विभेदक गुरुत्वाकर्षण) बल के कारण पुरस्सरण होता है। यह विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्यरेखीय उभार पर टॉर्क लगाता है और भूमध्यरेखीय उभार को चंद्रमा की कक्षा के तल के साथ संरेखित करने की कोशिश करता है, यदि कारण को चंद्रमा द्वारा अलग से माना जाता है। वास्तविकता में, यह विभिन्न कारणों के प्रभावों का अध्यारोपण होगा। चंद्रमा की कक्षा का तल क्रांतिवृत्त के 5 डिग्री के भीतर है और इसलिए इस टॉर्क का प्रभाव पृथ्वी के भूमध्यरेखीय तल को क्रांतिवृत्त के साथ मिलाना है। यदि पृथ्वी एक पूर्ण गोला होती (बिना भूमध्यरेखीय उभार के), तो कोई ज्वारीय बल नहीं होता और इसलिए चंद्रमा द्वारा कोई टॉर्क नहीं लगाया जाता। [एबेल, 1975; पेन - गैपोस्किन एंड हरमुंडानिस, 1970 ] ऊपर से देखने पर यह घूर्णन दक्षिणावर्त दिशा में होता है।
इस पुरस्सरण के कारण, दो विषुवों और संक्रांतियों से मिलकर बने बिंदुओं के समूह को जोड़ने वाली रेखाएं, क्रांतिवृत्त तल पर अपना अभिविन्यास बदलती हैं, जैसा कि चित्र 3A और 3B में दिखाया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा लगभग एक वृत्त है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्रमशः लगभग 152 और 147 मिलियन किलोमीटर है। पुरस्सरण के कारण, कैलेंडर महीनों के अनुसार विषुव पहले होते हैं। पुरस्सरण के कारण विषुव क्रांतिवृत्त पर पूर्व की ओर उसी दर से खिसकते हैं जिस दर से पुरस्सरण होता है। 25,800 वर्षों में 360 डिग्री से खिसकते हुए, हर साल वे (विषुव) क्रांतिवृत्त के साथ 50 सेकंड के चाप से पूर्व की ओर खिसकते हैं। उदाहरण के लिए, वसंत विषुव जो इन दिनों 21 मार्च को होता है, अतीत में अप्रैल में होता रहा होगा। इस चित्र में दिखाए गए अनुसार अन्य विषुव और संक्रांतियों के लिए भी इसी तरह के परिवर्तन होते हैं। चूँकि मौसम इन बिंदुओं पर निर्भर है, इसलिए मौसम भी उसी के अनुसार बदलते रहे हैं।
तालिका 1 में हिन्दू पद्धति के अनुसार महीनों और ऋतुओं को दर्शाया गया है, तथा इसमें पश्चिमी पद्धति के अनुसार उनके संगत नाम भी दर्शाए गए हैं।
पश्चिमी प्रणाली में भी, लोग समय बीतने और ऋतुओं में परिवर्तन को मापने के लिए राशियों पर निर्भर थे। यहाँ, क्रांतिवृत्त को 12 भागों में विभाजित किया गया था जहाँ प्रत्येक भाग की सीमा 30 डिग्री थी। विभिन्न राशियों को तालिका 2 में दिखाया गया है। पहले कॉलम में राशियों के नाम लिखे गए हैं, और उनके नीचे हिंदू प्रणाली में उपयोग की जाने वाली राशियाँ हैं (कोष्ठक में दर्शाई गई हैं)। दूसरा कॉलम इन राशियों के संक्षिप्त रूप दिखाता है। तीसरा और चौथा कॉलम क्रमशः राशियों और नक्षत्रों के विस्तार को दर्शाता है। पाँचवें कॉलम में संबंधित नक्षत्रों के नाम हैं। ये दोनों प्रणालियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं, और भाग 12 (राशि चिह्न) और 27 (नक्षत्र) का नीचे बताए गए के अलावा कोई संबंध नहीं है। भगवान ईसा मसीह के जन्म से पहले रचित ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण या ऋषि व्यास द्वारा रचित महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों में केवल नक्षत्रों का उल्लेख है।
आरंभिक नक्षत्र अश्विनी है, तथा यह राशि चक्र के आरंभिक चिन्ह मेष से संबंधित है। राशि चक्रों का यह विकास कब हुआ, यह ज्ञात नहीं है। मेष राशि ग्रीक सभ्यता के पनपने के समय पहली राशि थी - ऐसा इसलिए क्योंकि विषुव 2350 ई.पू. के आसपास मेष राशि के पहले बिंदु पर हुआ था। हालांकि, दोनों प्रणालियों के बीच एक मूलभूत अंतर है। हिंदू प्रणाली क्रांतिवृत्त पर नक्षत्रों के समूह की वास्तविक स्थिति पर आधारित है, लेकिन पश्चिमी ज्योतिषियों ने राशियों के नाम नहीं बदले, यद्यपि, पूर्वगमन के कारण, समय का वह क्षण जब एक कैलेंडर वर्ष में विषुव होता है, समय के साथ बदलता रहता है। यह पृथ्वी की कक्षा पर विभिन्न बिंदुओं पर होता है, जैसा कि चित्र 3ए और 3बी में दिखाया गया है। पश्चिमी ज्योतिष को - उष्णकटिबंधीय ज्योतिष कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मेष राशि का अर्थ हमेशा वसंत ऋतु की शुरुआत होगा, जबकि नक्षत्र - अश्विनी - में यह हमेशा सत्य नहीं होगा।
गुप्त काल - भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल [वोलपर्ट, 1993; त्रिपाठी, 1985]
इस अवधि में, विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान, भारत शास्त्रीय युग के शिखर पर पहुंच गया। गुप्त वंश के इस राजा के दरबार में कालिदास जैसे प्रसिद्ध कवि और कई खगोलशास्त्री थे, जो उज्जैन में स्थित था, एक शहर जिसे भारतीय खगोल विज्ञान में प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्राचीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान के स्कूल के बारे में आगे की चर्चा [जोसेफ, 2000] में देखी जा सकती है। जोसेफ के अनुसार, प्राचीन समय में खगोल विज्ञान का स्कूल पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) में स्थित था, जो मगध की राजधानी थी। इतिहास में इस शहर के कई नाम रहे हैं जैसे पाटलि, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर आदि। यह स्कूल उज्जैन में तब स्थानांतरित हुआ जब यह राजा अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन से शासन कर रहा था।
इस राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि उन्होंने 375 से 415 ई. के बीच शासन किया था, इसलिए सवाल उठता है - 57 ई.पू., युग की शुरुआत का नाम उनके नाम पर क्यों रखा गया?
लेखक के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसके दरबार के लोगों को यह अवश्य पता रहा होगा कि 57 ई.पू. में कुछ घटित हुआ था, अन्यथा वे उसके शासन काल के दौरान ही कोई समय चुन लेते।� लेकिन वह समय क्या हो सकता था, विशेषकर उनके समय से कई सौ वर्ष पूर्व?
चूँकि यह एक कैलेंडर से संबंधित था, जो उन दिनों एक खगोलीय घटना पर आधारित था, इसलिए तार्किक रूप से किसी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र को देखना होगा। खगोल विज्ञान पर पुस्तकों को पढ़ते हुए, लेखक ने एक घटना के बारे में सोचा - मेष से मीन राशि के बीच विषुव का संक्रमण (नक्षत्रों के अनुसार - यह अश्विनी से रेवती तक होगा)। इस संक्रमण को पंचांगम (राशि चक्र के 12 घरों में विभिन्न ग्रहों की स्थिति दिखाने के लिए हिंदुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक तालिका) पर विभिन्न सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके भी जांचा जा सकता है, अगर सॉफ़्टवेयर इतनी दूर की गणना कर सकता है। उनके दरबार में हिंदू खगोलविदों को पूर्वगामी घटना के बारे में पता था। इसलिए, उन्होंने समय के साथ इस संक्रमण घटना को विक्रम युग (संवत) की शुरुआत के रूप में नामित किया होगा।
यह सत्यापित करने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसा था, आइए तालिका 3 देखें जो 1000 ईसा पूर्व और 45 ईस्वी में अश्विनी और रेवती की औसत स्थिति दिखाती है [काये, 1981]। चूंकि इनमें से प्रत्येक नक्षत्र का विस्तार, डिग्री में, 13.333 डिग्री है, इसलिए किसी भी समय दो मानों का औसत संक्रमण की स्थिति देगा। इन दोनों नक्षत्रों की औसत स्थिति संक्रमण बिंदु के दोनों ओर 13.333 डिग्री के आधे से ऑफसेट होगी। तालिका 3 में दिखाया गया परिणाम (औसत) 358.39 डिग्री के बराबर है। यह 360 डिग्री के बहुत करीब है, और इसलिए, कोई भी सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाल सकता है कि यह वह घटना थी जो विक्रमादित्य के दरबार के खगोलविदों के दिमाग में थी। यह संक्रमण, विषुव पर सूर्य की स्थिति चित्र 4 [आचार, 2003] में भी देखी जा सकती है, जो आधुनिक तारामंडल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया आकाश मानचित्र है। इस चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सूर्य, विषुव पर, इन दो नक्षत्रों (अश्विनी और रेवती) के बीच स्थित है।
निष्कर्ष
इस शोध कार्य में, भारत के इतिहास को संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए देखा गया - विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से क्यों शुरू होता है? फिर, पश्चिमी और हिंदू प्रणालियों के खगोल विज्ञान की आवधिक गति के ज्ञान पर चर्चा की गई। अंत में, एक गणना द्वारा, प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ। उत्तर यह था कि - यह 57 ईसा पूर्व में नक्षत्रों - अश्विनी से रेवती के बीच संक्रमण था जो राशियों - मेष से मीन के बीच संक्रमण के अनुरूप है।
प्रतिक्रिया दें संदर्भ
एबेल, जी.ओ., 1975, "ब्रह्मांड की खोज", होल्ट, रिनहार्ट, और विंस्टन, टोरंटो, पृष्ठ 24; पृ.106-108.
आचार, एन, 2003, लेखक के साथ व्यक्तिगत संचार
बर्गेस, ई., 1977, "सूर्यसिद्धांत का अनुवाद: हिंदू खगोल विज्ञान की पाठ्यपुस्तक नोट्स और परिशिष्ट के साथ, इंडोलॉजिकल बुक हाउस, दिल्ली, पृ. 115 -120
देवी, एस., 1995, �एस्ट्रोलॉजी फॉर यू�, ओरिएंट पेपरबैक्स, नई दिल्ली, भारत
काये, जी., आर, 1981, 'हिंदू खगोल विज्ञान: हिंदुओं का प्राचीन विज्ञान' 'कॉस्मो प्रकाशन', नई दिल्ली, भारत, पृ. 119-120 .
पेन-गैपोस्किन, सी., और हरामुंडानिस, के., 1970, 'खगोल विज्ञान का परिचय', प्रेंटिस हॉल इंक, न्यू जर्सी, यू.एस.ए., अध्याय 1 से 7.
शास्त्री, बी.डी., और विल्किंसन, एल., 1974, "सूर्य सिद्धांत", फिलो प्रेस, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, अध्याय I, II और III.
त्रिपाठी, आर.एस., 1985, 'प्राचीन भारत का इतिहास', मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, भारत।
जोसेफ, जी, जी., 2000, 'द क्रेस्ट ऑफ द पीकॉक: नॉन-यूरोपियन रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स', प्रिंसटन, यू.एस.ए., अध्याय 8, और 9।
वोलपर्ट, एस., 1993, 'ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, यूएसए
तालिका 1: हिंदू कैलेंडर के महीने और ऋतुएँ
| हिन्दू माह | पश्चिमी महीने | हिन्दू ऋतु का नाम | पश्चिमी� ऋतु का नाम |
�1. | चैत्र | मार्च अप्रैल | वसंत | वसंत |
�2. | वैशाख | अप्रैल-मई | वसंत | वसंत |
�3. | ज्येष्ठ | मई-जून | ग्रीष्मा | गर्मी |
�4. | आषाढ़ | जून-जुलाई | ग्रीष्मा | गर्मी |
�5. | श्रावण | जुलाई-अगस्त | वर्षा | मानसून |
�6. | भाद्रपद | अगस्त सितम्बर | वर्षा | मानसून |
�7. | अश्विन | सितंबर-अक्टूबर | शरद | शरद ऋतु |
�8. | कार्तिक | अक्टूबर-नवंबर | शरद | शरद ऋतु |
�9. | मार्गशीर्ष | नवम्बर दिसम्बर | हेमंत | सर्दी |
10. | पौष | दिसंबर- जनवरी | हेमंत | सर्दी |
11। | माघ | जनवरी फ़रवरी | शिशिरा | डेवी |
12. | फाल्गुन | फरवरी-मार्च | शिशिरा | डेवी |
तालिका 2: राशियाँ और संबंधित नक्षत्र
राशि संकेत | संक्षिप्त रूप | कोण, राशि चक्र चिन्ह | कोण, नक्षत्र (डिग्री) | नक्षत्र (तारामंडल) |
एआरआईएस | एआर | 0 | 13.3333 | 1. अश्विनी |
(मेषा) |
|
| 26.6666 | 2. भरणी |
|
|
|
|
|
TAURUS | टा | 30 | 40 | 3. कृतिका |
(वृषभ) |
|
| 53.3333 | 4. रोहिणी |
|
|
|
|
|
मिथुन राशि | जीई | 60 | 66.6666 | 5. मृगशीर्ष |
(मिथुना) |
|
| 80 | 6. आर्द्रा |
|
|
|
|
|
कैंसर | सीए | 90 | 93.3333 | 7. पुनर्वसु |
(करकटा) |
|
| 106.666 | 8. पुष्य |
|
|
|
|
|
लियो | ले | 120 | 120 | 9. अश्लेषा |
( सिंहा) |
|
| 133.333 | 10. मघा |
|
|
| 146.666 | 11. पूर्वा फाल्गुनी |
|
|
|
|
|
कन्या | छठी | 150 | 160 | 12. उत्तरा फाल्गुनी |
(कन्या) |
|
| 173.333 | 13. हस्त |
|
|
|
|
|
तुला राशि | ली | 180 | 186.666 | 14. चित्रा |
(तुला) |
|
| 200 | 15. स्वाति |
|
|
|
|
|
वृश्चिक | अनुसूचित जाति | 210 | 213.333 | 16. विशाखा |
(वृश्चिक) |
|
| 226.666 | 17. अनुराधा |
|
|
|
|
|
धनुराशि | एसए | 240 | 240 | 18. ज्येष्ठ |
(धनु) |
|
| 253.333 | 19. मूला |
|
|
| 266.666 | 20. पूर्वाषाढ़ा |
|
|
|
|
|
मकर | सीपी | 270 | 280 | 21. उत्तराषाढ़ा |
(मकर) |
|
| 293.333 | 22. श्रवण |
|
|
|
|
|
कुंभ राशि | अक | 300 | 306.666 | 23. धनिष्ठा |
(कुंभ) |
|
| 320 | 24. शतभिषा |
|
|
|
|
|
मीन राशि | अनुकरणीय | 330 | 333.333 | 25. पूर्वा भाद्रपद |
(मीना) |
|
| 346.666 | 26. उत्तरा भाद्रपद |
|
|
| 360 | 27. रेवती |
तालिका 3: अश्विनी से रेवती नक्षत्र के बीच संक्रमण घटना [काये, 1981, पृ. 119-120]
तारा | नक्षत्र (तारांकन) | 1000 ई.पू. (डिग्री) ( दिया गया ) | 57 ई.पू., अंतर्वेशन द्वारा गणना (डिग्री) | 45 ई. (डिग्री) ( दिया गया ) |
. पिस्सियम | रेवती | 339.73 | 351.34 | 352.60 |
$ एरियेटिस | अश्विनी | 353.83 | 5.44 | 6.70 |
| औसत | 358.39 |
| |
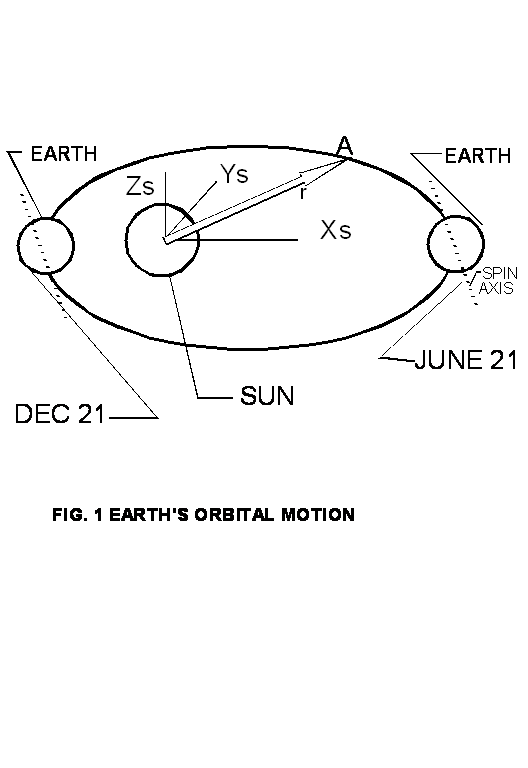 |
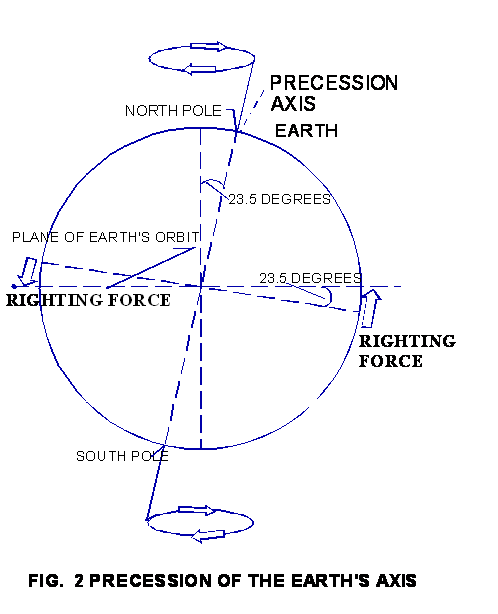 |
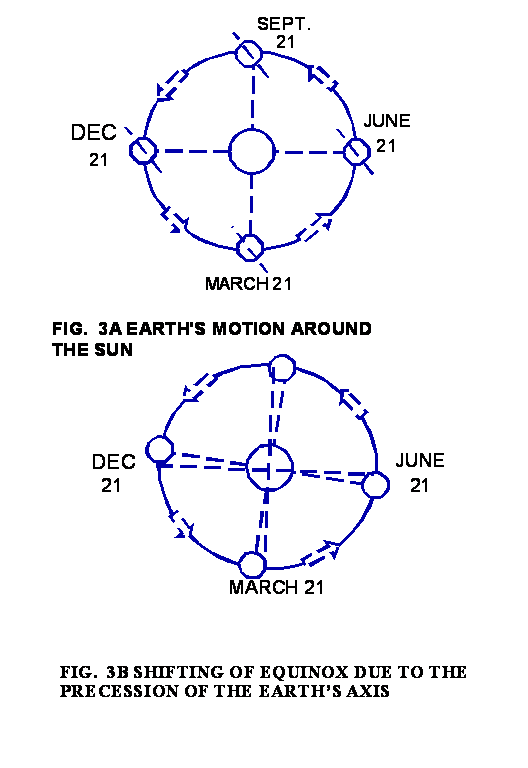 |
चित्र 4 57 ईसा पूर्व में विषुव पर नक्षत्रों का स्थान
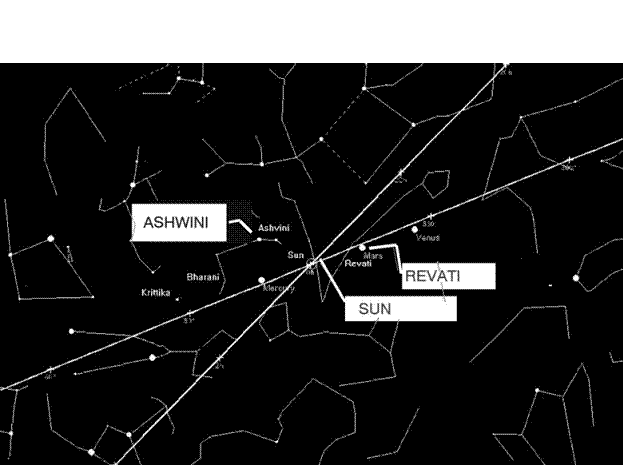 |


Comments
Post a Comment